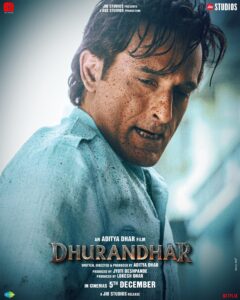धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत अधिकार है,सरकारी दखल नहीं

उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कई अहम सवाल पूछे हैं।
अदालत ने कहा कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाला लगता है और इससे सरकारी दखल बढ़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा —
“यह कानून उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है जो अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहते हैं।
धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद का मामला है, इसमें किसी सरकारी अधिकारी की दखल नहीं होनी चाहिए।”
बेंच ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून किसी व्यक्ति के धर्म बदलने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी की भूमिका बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जो कि व्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है।
अभी कानून की वैधता पर फैसला नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह इस कानून की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दे रही है।
हालांकि, अदालत ने यह ज़रूर माना कि धर्मांतरण से पहले और बाद में घोषणा करना अनिवार्य करना व्यक्ति के निजी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
“धर्म बदलना व्यक्तिगत अधिकार है”
बेंच ने कहा —
“कौन किस धर्म को मानता है, यह उसकी निजी पसंद है।
अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है, तो उसे यह सार्वजनिक रूप से बताने की क्या जरूरत है?
क्या यह उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है?”
अदालत ने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हर धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस जांच करवाने का निर्देश देना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है, जो कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए कहा कि —
“भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
भले ही ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 1976 में जोड़ा गया हो, लेकिन इसकी भावना संविधान में शुरू से मौजूद है।”
कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) का हवाला देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी भी कानून से कमजोर नहीं किया जा सकता।
नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपनी सोच, विश्वास और धर्म चुनने की पूरी स्वतंत्रता है।
“संविधान हमें सोचने, बोलने और विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था बदलना चाहता है, तो यह उसका अधिकार है।
सरकार का काम इस पर निगरानी रखना नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।”
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि
भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर नागरिक को अपनी आस्था और विचार चुनने की आज़ादी मिले।
धर्म परिवर्तन का अधिकार निजता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है —
और किसी भी कानून को इस पर अनुचित रोक नहीं लगानी चाहिए।

News World India is India’s Fastest Growing News channel known for its quality programs, authentic news, and reliable breaking news. News World India brings you 24/7 Live Streaming, Headlines, Bulletins, Talk Shows, Infotainment, and much more.
Watch minute-by-minute updates of current affairs and happenings from India and all around the world!